Free solutions for UP Board class 9 Hindi Padya chapter 1 – “साखी” are available here. These solutions are prepared by the subject experts and cover all question answers of this chapter for free.
उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में “साखी” नामक पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में महान संत कवि कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन है। साखी दरअसल कबीर के दोहे हैं, जो गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश देते हैं। इन साखियों में कबीर ने सरल भाषा में जीवन के मूल्यवान सिद्धांतों को समझाया है। वे गुरु की महिमा, ईश्वर-प्रेम, और मायावी संसार से मुक्ति जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हैं।
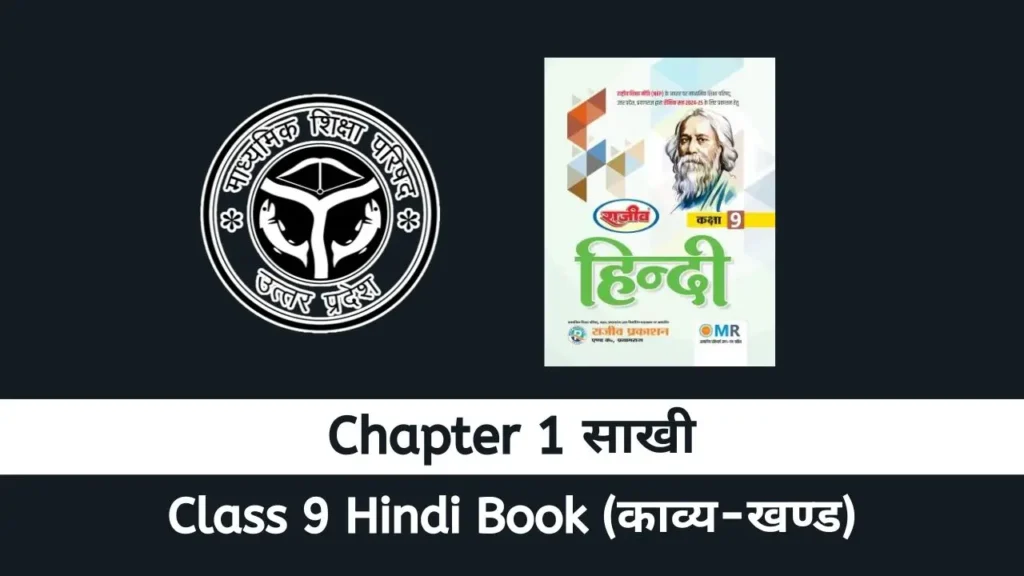
UP Board Class 9 Hindi Padya Chapter 1 Solution
Contents
| Subject | Hindi (काव्य खंड) |
| Class | 9th |
| Chapter | 1. साखी |
| Author | कबीरदास |
| Board | UP Board |
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. निम्नलिखित पद्यांशों की ससन्दर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौन्दर्य भी स्पष्ट कीजिए :
(अ) सतगुरु हम सँ…………………….भीजि गया सब अंग।
उत्तर-
- सन्दर्भ- प्रस्तुत साखी संत कबीर द्वारा रचित है, जो हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी काव्य’ में संकलित है।
- प्रसंग- इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता और उनके द्वारा दिए गए उपदेश की बात की है, जो आत्मा में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जाग्रत करता है।
- व्याख्या- कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी सेवा-भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। यह उपदेश मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न कर गया, जैसे प्रेमरूपी बादल से जल बरस रहा हो और मेरा तन-मन उस प्रेम में भीग गया हो। कबीर के अनुसार, गुरु के बिना ईश्वर का प्रेम संभव नहीं है और वही प्रेम आत्मा को शांति प्रदान करता है। गुरु का जीवन में महत्त्व अत्यधिक होता है क्योंकि वे जीवन की दिशा बदलने में सहायक होते हैं।
- काव्यगत सौन्दर्य: भाषा सधुक्कड़ी है। छन्द दोहा है। अलंकार रूपक है। रस शान्त है।
(ब) माया दीपक……………………………… उबरंत।
उत्तर-
- सन्दर्भ– यह साखी संत कबीर द्वारा रचित है और हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी काव्य’ में संकलित है।
- प्रसंग– इस साखी में कबीरदास ने माया और जीव के संबंध को दीपक और पतंगा का रूपक देकर समझाया है।
- व्याख्या– कबीर कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है, जो अपनी चमक से जीवों को आकर्षित करता है। मनुष्य उस माया के जाल में फंसकर अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है, जैसे पतंगा दीपक के पास जाकर जल जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, जो गुरु के उपदेश से इस माया के जाल से बच पाते हैं। गुरु के उपदेश का महत्त्व यहां स्पष्ट रूप से दिखाया गया है।
- काव्यगत सौन्दर्य: भाषा सधुक्कड़ी है। छन्द दोहा है। अलंकार अनुप्रास है। रस शान्त है।
(स) अंषड़ियाँ झाईं पड़ी ………………………………. राम पुकारि-पुकारि।
उत्तर-
- सन्दर्भ– यह साखी संत कबीर द्वारा रचित है और हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी काव्य’ में संकलित है।
- प्रसंग– इस दोहे में कबीरदास ने जीवात्मा के विरह की पीड़ा को व्यक्त किया है।
- व्याख्या– कबीर कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में इतनी व्याकुल हो जाती है कि उसकी आँखों में झाइयाँ पड़ जाती हैं। भगवान का नाम जपते-जपते उसकी जीभ में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी उसे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। केवल नाम जपने से ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है, जब तक हृदय में सच्ची भक्ति न हो।
- काव्यगत सौन्दर्य: भाषा सधुक्कड़ी है। छन्द दोहा है। रस शान्त है। अलंकार पुनरुक्तिप्रकाश और अनुप्रास है।
(द) यहुँ ऐसा संसार………………………………………………… न भूलि।
उत्तर-
- सन्दर्भ– प्रस्तुत साखी संत कबीर द्वारा रचित है और ‘हिन्दी काव्य’ में संकलित है।
- प्रसंग- इस साखी में कबीरदास ने संसार की असारता को समझाते हुए बताया है कि सांसारिक माया में उलझने का कोई अर्थ नहीं है।
- व्याख्या– कबीर कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह दिखने में आकर्षक और सुंदर तो है, परंतु इसके अंदर कोई वास्तविक गुण नहीं है। जैसे तोता इस फूल की सुंदरता से प्रभावित होकर उसमें रस खोजता है, परंतु अंत में उसे केवल रुई ही मिलती है, वैसे ही यह संसार भी केवल बाहरी दिखावा है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस झूठे आकर्षण में न फंसे और सच्चाई की ओर ध्यान दे।
- काव्यगत सौन्दर्य: भाषा सधुक्कड़ी है। छन्द दोहा है। रस शान्त है। अलंकार उपमा है।
(य) यह तन काचा ………………………………………………… आया हाथि।
उत्तर-
- सन्दर्भ– प्रस्तुत साखी संत कबीर द्वारा रचित है और हमारी पाठ्य-पुस्तक ‘हिन्दी काव्य’ में संकलित है।
- प्रसंग– इस साखी में कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है।
- व्याख्या– कबीर कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है। परंतु जैसे कच्चा घड़ा एक छोटे से धक्के से टूट जाता है, वैसे ही यह शरीर भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। मनुष्य को इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह क्षणभंगुर है और अंत में यह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें इस नश्वरता को समझते हुए जीवन जीना चाहिए।
- काव्यगत सौन्दर्य: भाषा सधुक्कड़ी है। छन्द दोहा है। रस शान्त है। अलंकार रूपक और अनुप्रास है।
प्रश्न 2. कबीरदास का जीवन-परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए।
अथवा, कबीर का जीवन-परिचय बताते हुए उनकी साहित्यिक सेवाओं पर प्रकाश डालिए।
अथवा, कबीर की भाषा-शैली स्पष्ट कीजिए।
उत्तर- कबीरदास का जीवन-परिचय एवं उनकी साहित्यिक सेवाएँ:
कबीरदास 15वीं शताब्दी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म काशी (वर्तमान वाराणसी) में हुआ था। वे बचपन से ही साधु-संतों के संपर्क में रहे और संत रामानंद उनके गुरु माने जाते हैं। कबीरदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता का विरोध किया और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और पाखंडों की आलोचना की। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, जिनका संदेश था कि ईश्वर का सच्चा रूप बिना किसी रूप या मूर्ति के भी अनुभव किया जा सकता है।
कबीर की रचनाओं में ‘बीजक’, ‘साखी’, ‘रमैनी’, और ‘सबद’ प्रमुख हैं। उनकी भाषा सधुक्कड़ी, सरल, और जनसाधारण के लिए समझने योग्य थी। उन्होंने अपने पदों और दोहों में खड़ीबोली, अवधी, ब्रजभाषा, और पंजाबी का प्रयोग किया। उनकी रचनाएँ समाज में प्रेम, एकता और सत्य का संदेश देती हैं। कबीरदास की साहित्यिक सेवा का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने समाज को जाति-पाति और धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया। उनका साहित्य आज भी लोगों को सच्चे ज्ञान और भक्ति की ओर प्रेरित करता है।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. मोक्ष प्राप्त करने के लिए कबीर ने किन साधनों को अपनाने का उपदेश दिया है?
उत्तर- कबीर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन को वश में रखने, लोभ, मोह और भ्रम का त्याग करने का उपदेश दिया है। उन्होंने सत्संगति, गुरु के मार्गदर्शन और मन की दृढ़ता पर बल दिया है। उनका मानना था कि सही साधन अपनाकर ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
प्रश्न 2. कबीर के समाज-सुधार पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए।
उत्तर- कबीरदास ने समाज में फैली धार्मिक कट्टरता और भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त पाखंडों की आलोचना की। उनका संदेश था कि मनुष्य को आपसी भेदभाव छोड़कर सच्चाई, प्रेम और एकता का मार्ग अपनाना चाहिए।
प्रश्न 3. कबीर के काव्य की मुख्य विशेषताएँ बताइए।
उत्तर- कबीर का काव्य सरल, स्पष्ट और समाज सुधारक दृष्टिकोण को दर्शाने वाला है। उनकी कविताओं में सामाजिक कुरीतियों का विरोध और ज्ञान का प्रचार मिलता है। वे अपने काव्य के माध्यम से समाज में सुधार और सत्य का प्रचार करते थे।
प्रश्न 4. कबीर की भाषा का उल्लेख कीजिए।
उत्तर- कबीर की भाषा सधुक्कड़ी कहलाती है, जिसमें कई भाषाओं और बोलियों का मिश्रण है। उन्होंने अरबी, फारसी, भोजपुरी, अवधी और ब्रज जैसी भाषाओं के शब्दों का सरलता से प्रयोग किया। उनकी भाषा में स्पष्टता और सच्चाई के साथ भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता है।
प्रश्न 5. कबीर के अनुसार जीवन में गुरु के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर- कबीर के अनुसार गुरु का जीवन में अत्यधिक महत्त्व है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। वे गुरु को ईश्वर के समान मानते थे और कहते थे कि बिना गुरु के जीवन अधूरा है।
प्रश्न 6. कबीर ने संसार को सेमल के फूल के समान क्यों कहा है?
उत्तर- कबीर ने संसार को सेमल के फूल के समान इसलिए कहा क्योंकि यह दिखने में आकर्षक है, परंतु इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। जैसे सेमल का फूल गंधहीन और क्षणिक होता है, वैसे ही संसार की सुख-सुविधाएँ भी क्षणिक और असार हैं।
प्रश्न 7. कबीर मनुष्य को गर्व न करने का उपदेश क्यों देते हैं?
उत्तर- कबीर ने मनुष्य को गर्व न करने का उपदेश इसलिए दिया क्योंकि संसार की हर वस्तु नश्वर है। मनुष्य जिस धन, शक्ति और सुख-सुविधाओं पर गर्व करता है, वे सब अंततः मिट जाती हैं। गर्व केवल मोह-माया में फंसाने का कारण बनता है।
प्रश्न 8. सतगुरु की सरस बातों का कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर- सतगुरु की सरस बातों ने कबीर के हृदय में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम पैदा कर दिया। उनके मन और शरीर में एक अलौकिक शांति और भक्ति का भाव भर गया।
प्रश्न 9. कबीर की रचना में से ऐसी दो पंक्तियाँ खोजकर लिखिए जिनमें उन्होंने अहंकार को नष्ट करने का उपदेश दिया है।
उत्तर- कबीर की रचना की पंक्तियाँ हैं:
“मैमंता मन मारि रे, न हां करि करि पीसि।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं।”
इन पंक्तियों में कबीर ने अहंकार को नष्ट करने और ईश्वर की भक्ति में लीन होने का संदेश दिया है।
अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. भक्तिकाल के किसी एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए।
उत्तर- भक्तिकाल के प्रमुख कवि संत कबीरदास जी हैं, और उनकी प्रसिद्ध रचना “साखी” है।
प्रश्न 2. कबीर किस धर्म के पोषक थे?
उत्तर- कबीरदास जी हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के आदर्शों के समर्थक थे। वे धर्म के नाम पर भेदभाव का विरोध करते थे और मानवता को सर्वोपरि मानते थे।
प्रश्न 3. कबीर उस घर को कैसा बताते हैं जहाँ न तो साधु की पूजा होती है और न ही हरि की सेवा।
उत्तर- कबीरदास जी के अनुसार, वह घर जहाँ साधु का सम्मान और ईश्वर की भक्ति नहीं होती, मरघट के समान है। ऐसे घर में नकारात्मकता और अज्ञानता का वास होता है।
प्रश्न 4. निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही (✓) का चिह्न लगाइए –
(अ) कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे। (✓)
(ब) साखी चौपाई छन्द में लिखा गया है। (✘)
(स) रावण के सवा लाख पूत थे। (✓)
(द) कबीर को लालन-पालन नीमा और नीरू ने किया था। (✘)
प्रश्न 5. कबीर किस काल के कवि हैं?
उत्तर- कबीर भक्तिकाल के कवि हैं।
प्रश्न 6. कबीर कैसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं?
उत्तर- कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मधुर और शीतल हो। इससे न केवल स्वयं को शांति मिलती है, बल्कि दूसरों को भी सुख और शांति का अनुभव होता है।
प्रश्न 7. कबीर का जन्म एवं मृत्यु संवत् बताइए।
उत्तर- कबीरदास जी का जन्म संवत् 1455 विक्रमी में हुआ और उनकी मृत्यु संवत् 1575 विक्रमी में हुई।
प्रश्न 8. ‘साखी’ किस छन्द में लिखा गया है?
उत्तर- ‘साखी’ दोहा छंद में लिखा गया है।
प्रश्न 9. कबीर की भाषा-शैली की मुख्य विशेषताएँ बताइए।
उत्तर- कबीर की भाषा को ‘सधुक्कड़ी’ या ‘पंचमेल खिचड़ी’ कहा जाता है क्योंकि इसमें खड़ीबोली, ब्रज, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, और बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्दों का मेल है। उनकी भाषा सरल, सहज और स्पष्ट है, जिससे उनके उपदेश आम जनता के लिए आसानी से समझने योग्य होते हैं। कबीर ने दोहा, चौपाई और पद शैली का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, जिससे उनकी रचनाएँ भावनात्मक और व्यंग्यात्मक हो गईं।
प्रश्न 10. कबीर की रचनाओं की सूची बनाइए।
उत्तर- कबीर की प्रमुख रचनाएँ हैं: साखी, सबद, और रमैनी।
काव्य-सौन्दर्य एवं व्याकरण-बोध
प्रश्न 1. निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए
ग्यान, अंधियार, सैंबल, भगति, दुक्ख, व्योहार
- ग्यान – ज्ञान
- अंधियार – अंधकार
- सैंबल – सेमल
- भगति – भक्ति
- दुक्ख – दुःख
- व्योहार – व्यवहार
प्रश्न 2. निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार एवं छन्द बताइए l
(अ) सतगुरु हम सँ रीझि कर, एक कह्या प्रसंग।
(ब) माया दीपक नर पतंग, भ्रमि, भ्रमि इवै पड्त।
(स) यहुँ ऐसा संसार है, जैसा सैंबल फूल ।
उत्तर-
(अ) इसमें रूपक अलंकार है तथा दोहा छन्द है।
(ब) इस पंक्ति में अन्त्यानुप्रास अलंकार तथा दोहा छन्द है।
(स) इस पंक्ति में रूपक तथा उपमा अलंकार है।
प्रश्न 3. ‘जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं’ पंक्ति का काव्य-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।
उत्तर- काव्य-सौन्दर्य-
- यहाँ कवि का सन्देश है कि ईश्वर प्रेम के लिए अहम् को त्यागना ही पड़ता है।
- भाषा-पंचमेल खिचड़ी।
- शैली-आलंकारिक।
- रस-शान्त तथा भक्ति।
- छन्द-दोहा (साखी) ।
