UP Board Class 9 History chapter 6 solutions are available for free on this page. It is prepared by the subject experts and brings you the complete question answer of chapter 6 – “किसान और काश्तकार” in hindi medium.
इस अध्याय में आप भारतीय कृषि समाज के दो महत्वपूर्ण वर्गों – किसानों और काश्तकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह अध्याय आपको बताएगा कि ये दोनों वर्ग एक-दूसरे से कैसे भिन्न हैं और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी क्या भूमिका है। आप समझेंगे कि कैसे औपनिवेशिक काल में भूमि व्यवस्था में परिवर्तनों ने इन वर्गों को प्रभावित किया और उनके जीवन में क्या बदलाव आए। इसके अलावा, आप स्वतंत्रता के बाद की भूमि सुधार नीतियों और उनके प्रभावों के बारे में भी पढ़ेंगे।
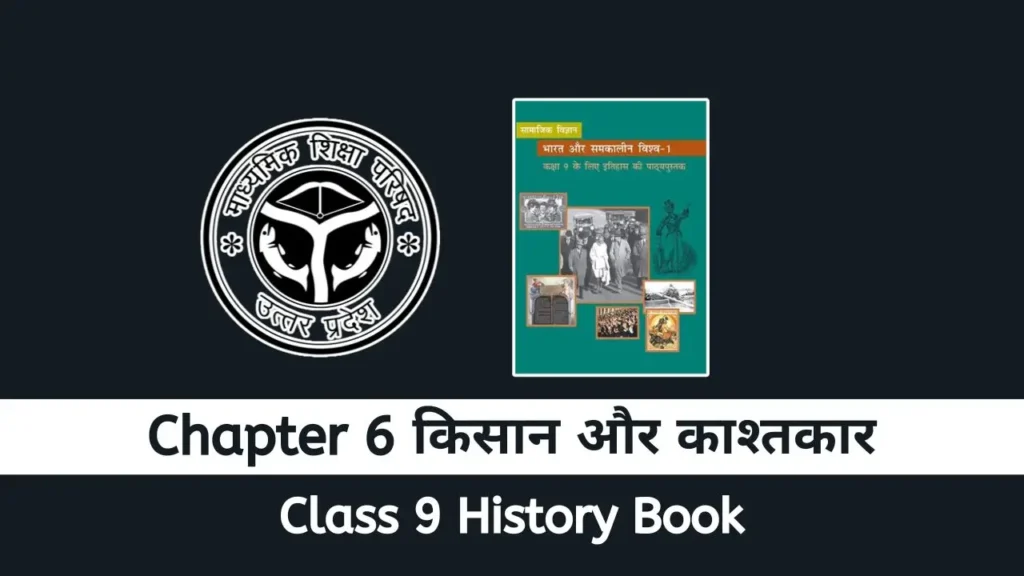
UP Board Class 9 History Chapter 6 Solutions
| Subject | History |
| Class | 9th |
| Chapter | 6. किसान और काश्तकार |
| Board | UP Board |
किसान और काश्तकार Question Answer
प्रश्न 1. अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड की ग्रामीण जनता खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखती थी। संक्षेप में व्याख्या करें।
इस व्यवस्था को-
- एक संपन्न किसान,
- एक मजदूर,
- एक खेतिहर स्त्री।
उत्तर:-
एक संपन्न किसान की दृष्टि में:
संपन्न किसान खुले खेतों को अपने लाभ का साधन मानते थे। वे अपने पशुओं के लिए अच्छी चरागाह चाहते थे। इसलिए उन्होंने साझा भूमि पर बाड़ लगानी शुरू कर दी। वे गरीब लोगों को इन भूमियों से दूर रखना चाहते थे। बाद में, सरकार ने भी इस व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी।
एक मजदूर की दृष्टि में:
गरीब मजदूरों के लिए साझा भूमि बहुत महत्वपूर्ण थी। वे यहाँ अपने जानवर चराते थे। वे लकड़ी इकट्ठा करते और कंद-मूल खोजते थे। नदियों में मछली पकड़ना और जंगलों में शिकार करना उनके जीवन का हिस्सा था। खुले खेतों के बंद होने से उनका जीवन कठिन हो गया।
एक खेतिहर स्त्री की दृष्टि में:
खेतिहर महिलाएँ अपने परिवार के साथ खुले खेतों में काम करती थीं। वे साझा भूमि से ईंधन इकट्ठा करती थीं और पशुओं की देखभाल में मदद करती थीं। साझा भूमि उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत थी। बाड़बंदी के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वे अब पहले की तरह संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकती थीं।
प्रश्न 2. इंग्लैण्ड में हुए बाड़बंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करें।
उत्तर:- इंग्लैंड में बाड़बंदी आंदोलन कई कारणों से हुआ:-
- बेहतर कृषि: किसान अपने खेतों को बाड़ से घेरकर बेहतर फसलें उगाना चाहते थे। वे नई तकनीकों का उपयोग करके अधिक उपज पाना चाहते थे।
- पशुपालन में सुधार: संपन्न किसान अपने पशुओं के लिए अच्छी चरागाह चाहते थे। वे अपने पशुओं को दूसरों के पशुओं से अलग रखना चाहते थे।
- ऊन का व्यापार: ऊन की कीमतें बढ़ने से किसान अधिक भेड़ें पालना चाहते थे। इसके लिए उन्हें बड़े चरागाहों की जरूरत थी।
- जनसंख्या वृद्धि: बढ़ती जनसंख्या के कारण अनाज की माँग बढ़ गई। किसान अधिक अनाज उगाने के लिए अपनी भूमि को बाड़ से घेरना चाहते थे।
- निजी संपत्ति: संपन्न किसान साझा भूमि पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वे इन भूमियों को अपनी निजी संपत्ति बनाना चाहते थे।
प्रश्न 3. इंग्लैण्ड के गरीब किसान थेसिंग मशीन का विरोध क्यों कर रहे थे?
उत्तर:- इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेशिंग मशीन का विरोध कई कारणों से कर रहे थे। मुख्य रूप से, इन मशीनों ने उनके रोजगार और आजीविका को खतरे में डाल दिया था। थ्रेशिंग मशीनों के आने से फसल कटाई के दौरान मजदूरों की आवश्यकता कम हो गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। पहले, मजदूर पूरे वर्ष विभिन्न कृषि कार्यों में लगे रहते थे, लेकिन अब उन्हें केवल फसल कटाई के समय ही काम मिलता था। इसके अलावा, नेपोलियन युद्धों के बाद लौटे सैनिकों के लिए भी रोजगार की कमी थी, और मशीनीकरण ने इस समस्या को और बढ़ा दिया।
मशीनीकरण ने ग्रामीण समाज के परंपरागत ढांचे को भी बदल दिया, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ा। बड़े भूस्वामियों को लाभ हुआ, जबकि छोटे किसान और मजदूर पीछे छूट गए, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी। इन सभी कारणों से गरीब किसानों और मजदूरों ने थ्रेशिंग मशीनों का विरोध किया, जो उनके लिए न केवल आजीविका बल्कि सामाजिक स्थिरता के लिए भी खतरा बन गई थीं।
प्रश्न 4. कैप्टन स्विंग कौन था? यह नाम किस बात का प्रतीक था और वह किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था?
उत्तर:- कैप्टन स्विंग 1830 के दशक में इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए किसान विद्रोह से जुड़ा एक काल्पनिक नाम था। यह नाम कृषि मशीनीकरण और भूस्वामियों के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक बन गया था। विद्रोहियों ने अपनी पहचान छिपाने और विभिन्न क्षेत्रों के असंतुष्ट किसानों और मजदूरों को एकजुट करने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया। कैप्टन स्विंग के नाम से भेजे गए पत्र भूस्वामियों को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और यह बेहतर मजदूरी और काम की स्थितियों की मांग का प्रतीक था। यह नाम मुख्य रूप से भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों, ग्रामीण कारीगरों, बेरोजगार ग्रामीण आबादी और कृषि में मशीनीकरण से प्रभावित लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। कैप्टन स्विंग आंदोलन ग्रामीण इंग्लैंड में बढ़ती आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी, जो मशीनीकरण और बदलती आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न हुई थी।
प्रश्न 5. अमेरिका पर नए अप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार को क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर:- अमेरिका में नए अप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार ने देश के भूगोल, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। पर्यावरण पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ा, क्योंकि वनों और घास के मैदानों को कृषि भूमि में बदल दिया गया, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ा और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में धूल भरी आंधियां और वर्षा में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। इस विस्तार ने अमेरिकी मूल निवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया, जिससे उनकी संस्कृति और जीवन शैली प्रभावित हुई। हालांकि, इसने कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि की, जिससे अमेरिका विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश बन गया। नए क्षेत्रों के विकास से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिला, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई।
पश्चिमी क्षेत्रों में नए शहरों और बस्तियों का विकास हुआ, जिससे देश की जनसंख्या का वितरण बदला। प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन शुरू हुआ, और विभिन्न पृष्ठभूमि के अप्रवासियों के आगमन से अमेरिकी संस्कृति और समाज अधिक विविध बना।
प्रश्न 6. अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन के फायदे-नुकसान क्या-क्या थे?
उत्तर:- अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए, जिनके कई फायदे और नुकसान थे। फायदों में, इन मशीनों ने गेहूं उत्पादन में तेज वृद्धि की, जिससे अमेरिका विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक बना। साइरस मैककार्मिक की मशीन जैसी नवीन तकनीकों ने समय और श्रम की बचत की, जिससे बड़े पैमाने पर खेती संभव हुई। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। हालांकि, इन मशीनों के कई नकारात्मक प्रभाव भी थे। महंगी मशीनें खरीदने के लिए लिए गए ऋण और गेहूं की मांग में अचानक गिरावट ने कई छोटे किसानों को बर्बाद कर दिया।
मशीनीकरण ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को कम कर दिया, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ी। बड़े किसान लाभान्वित हुए, जबकि छोटे किसान और मजदूर पीछे छूट गए, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी। परंपरागत कृषि प्रथाओं के बदलने से ग्रामीण समुदायों की सामाजिक संरचना प्रभावित हुई। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर एकल फसल की खेती ने मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता को प्रभावित किया। इस प्रकार, फसल काटने वाली मशीनों ने जहां कृषि उत्पादकता को बढ़ाया, वहीं उन्होंने कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी पैदा कीं।
प्रश्न 7. अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं?
उत्तर:- अमेरिका में गेहूं की खेती के उछाल और उसके बाद पैदा हुए पर्यावरण संकट से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे पहले, यह घटना दिखाती है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। गेहूं उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वनों और घास के मैदानों को नष्ट किया गया, जिसने पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप, दक्षिण-पश्चिम अमेरिका में धूल के तूफान और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुईं।
यह घटना हमें सिखाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है। अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण की अनदेखी करना अंततः मानव और पशु जीवन के लिए घातक हो सकता है। इसलिए, विकास की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए।
हमें यह भी सीखना चाहिए कि कृषि प्रथाओं में विविधता और स्थायित्व महत्वपूर्ण है। एक ही फसल पर अत्यधिक निर्भरता मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर सकती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बजाय, फसल चक्र और जैविक खेती जैसी टिकाऊ कृषि तकनीकों को अपनाना चाहिए।
अंत में, यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और मानव गतिविधियों के बीच एक नाजुक संतुलन है। हमें विकास के ऐसे मॉडल अपनाने चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करें। यह सीख न केवल कृषि के लिए, बल्कि सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रासंगिक है।
प्रश्न 8. अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे थे?
उत्तर:- अंग्रेज भारतीय किसानों पर अफीम की खेती के लिए दबाव डाल रहे थे क्योंकि यह उनकी आर्थिक और व्यापारिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहले, भारत की जलवायु और मिट्टी अफीम की खेती के लिए बहुत उपयुक्त थी, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली अफीम का उत्पादन संभव था।
दूसरा प्रमुख कारण चीन के साथ व्यापार संतुलन था। इंग्लैंड में चाय की बढ़ती लोकप्रियता के कारण, अंग्रेजों को चीन से बड़ी मात्रा में चाय खरीदनी पड़ती थी। हालांकि, चीन इंग्लिश वस्तुओं में रुचि नहीं रखता था, जिससे व्यापार असंतुलन पैदा हो रहा था। इस समस्या का समाधान अंग्रेजों ने भारतीय अफीम में पाया।
अंग्रेज भारत में उत्पादित अफीम को चीन में बेचते थे, जहां इसकी मांग बहुत अधिक थी। इस व्यापार से प्राप्त आय का उपयोग वे चीन से चाय खरीदने के लिए करते थे। यह रणनीति उन्हें चांदी के बहिर्वाह को रोकने में मदद करती थी, जो अन्यथा चाय के भुगतान में जाती।
इस प्रकार, अफीम व्यापार अंग्रेजों के लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा था। यह न केवल उन्हें चीन के साथ व्यापार संतुलन बनाए रखने में मदद करता था, बल्कि भारत में उनके शासन के लिए महत्वपूर्ण राजस्व भी प्रदान करता था। इसलिए, वे भारतीय किसानों पर अफीम की खेती के लिए लगातार दबाव डालते रहे, भले ही इसका किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
प्रश्न 9. भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे?
उत्तर:- भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति उदासीन थे क्योंकि यह उनके लिए कई तरह से अलाभकारी और समस्याग्रस्त थी। सबसे पहले, अफीम की खेती के लिए सबसे उपजाऊ और गांव के निकट की भूमि की आवश्यकता होती थी। ऐसी भूमि के लिए जमींदार बहुत अधिक किराया वसूल करते थे, जो छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए बोझ बन जाता था।
दूसरा, अफीम की खेती खाद्य फसलों, विशेष रूप से दालों की खेती के स्थान पर की जाती थी। इससे किसानों के लिए अपने परिवार के भोजन की आपूर्ति करना मुश्किल हो जाता था और स्थानीय खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती थी।
तीसरा, अफीम की खेती एक श्रम-गहन और जटिल प्रक्रिया थी। अफीम का पौधा बहुत नाजुक होता है और इसे लगातार देखभाल की आवश्यकता होती है। इससे किसानों के पास अन्य आवश्यक कृषि गतिविधियों के लिए समय कम बच पाता था।
चौथा, और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार किसानों को अफीम का बहुत कम मूल्य देती थी। यह मूल्य इतना कम होता था कि किसानों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता था। अफीम व्यापार से होने वाला अधिकांश लाभ अंग्रेजों के पास जाता था, जबकि किसान मुश्किल से अपनी लागत निकाल पाते थे।
इन कारणों से, भारतीय किसान अफीम की खेती को अपने हित में नहीं मानते थे। वे इसे एक बोझ और शोषण का माध्यम समझते थे, जो उन्हें अपनी पारंपरिक और अधिक टिकाऊ कृषि प्रथाओं से दूर ले जा रहा था। इसलिए, वे इस फसल के प्रति उदासीन रहते थे और जहां संभव हो, इसकी खेती से बचने का प्रयास करते थे।
