On this page we have shared the written Solutions for Bihar Board Class 8 History Chapter 3 – “ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना”. These solutions are prepared by the subject experts and follows the new syllabus of Bihar Board. All question-answers are in Hindi medium.
यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी हासिल करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अपना शासन चलाया। हम जानेंगे कि कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त, महालवारी और रैयतवारी जैसे तरीकों से किसानों और ज़मींदारों से राजस्व वसूला। यह भी समझ आएगा कि नील और अफ़ीम जैसी फसलों की खेती ने किसानों की जिंदगी को मुश्किल बनाया और नील विद्रोह जैसे आंदोलनों की शुरुआत हुई। इस अध्याय से आपको कंपनी के शासन और ग्रामीण जीवन पर इसके प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी।
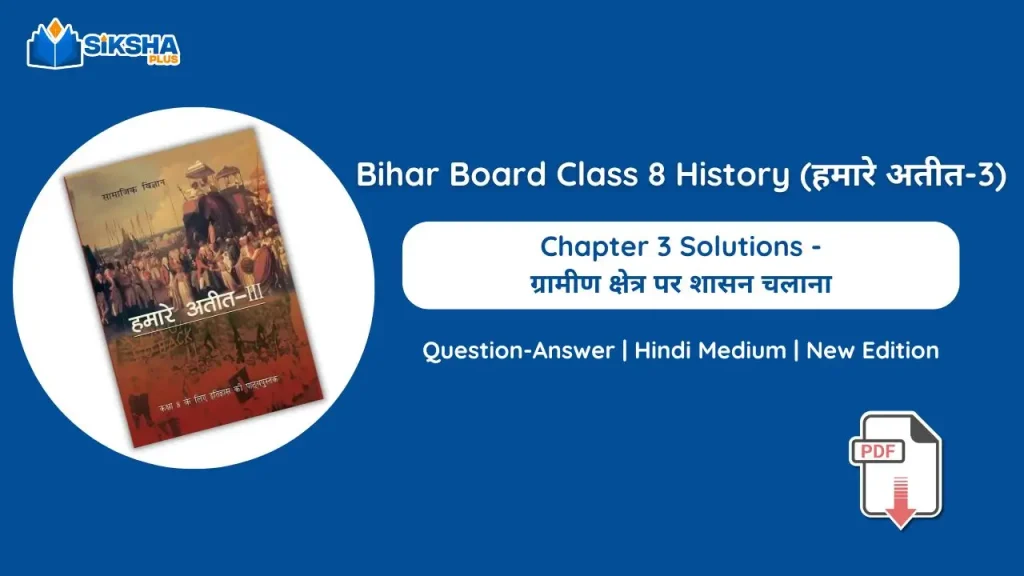
Bihar Board Class 8 History Chapter 3 Solutions
Contents
| Subject | History (हमारे अतीत-3) |
| Chapter | 3. ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना |
| Class | 8th |
| Board | Bihar Board |
फिर से याद करें
1. निम्नलिखित के जोड़े बनाएँ-
उत्तर:
- रैयत – किसान
- महाल – ग्राम-समूह
- निज – बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती
- रैयती – रैयतों की ज़मीन पर खेती
2. रिक्त स्थान भरें-
(क) यूरोप में नील उत्पादकों को …………… से अपनी आमदनी में गिरावट का ख़तरा दिखाई देता था।
उत्तर: नील।
(ख) अठारहवीं सदी के आख़िर में ब्रिटेन में नील की माँग …………… के कारण बढ़ने लगी।
उत्तर: औद्योगिकरण।
(ग) …………… की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय माँग पर बुरा असर पड़ा।
उत्तर: कृत्रिम रंग।
(घ) चंपारण आंदोलन …………… के ख़िलाफ़ था।
उत्तर: नील बागान मालिकों।
आइए विचार करें
3. स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर: स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया। इसके मुख्य पहलू इस प्रकार थे:
- स्थायी राजस्व: कंपनी ने जमींदारों के लिए एक निश्चित राशि तय की, जो उन्हें हर साल सरकार को देनी थी। यह राशि कभी नहीं बदलती थी।
- जमींदारों की जिम्मेदारी: जमींदारों को किसानों से कर वसूलने और उसे कंपनी को देने का काम सौंपा गया।
- जमीन पर सुधार की कमी: राजस्व की राशि इतनी ज्यादा थी कि जमींदार जमीन को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाते थे।
- जमींदारी छिनना: अगर जमींदार समय पर राजस्व नहीं दे पाते, तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी और उसे नीलाम कर दिया जाता था।
4. महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी?
उत्तर: महालवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में ये मुख्य अंतर थे:
| महालवारी व्यवस्था | स्थायी बंदोबस्त |
|---|---|
| 1822 में होल्ट मैकेंजी ने उत्तर-पश्चिमी प्रांतों में शुरू की। | 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की। |
| राजस्व अस्थायी था और समय-समय पर बदला जा सकता था। | राजस्व स्थायी था, उसमें कोई बदलाव नहीं होता था। |
| गाँव के मुखिया को राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। | जमींदारों को राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। |
| जमीन की माप और फसलों का आकलन किया जाता था। | किसानों के अधिकारों की अनदेखी की गई और जमींदारों का दबदबा बढ़ा। |
5. राजस्व निर्धारण की नयी मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएँ बताइए।
उत्तर: मुनरो व्यवस्था के कारण दो मुख्य समस्याएँ थीं:
- उच्च राजस्व दर: राजस्व की राशि बहुत ज्यादा थी। किसान इतना अधिक कर नहीं दे पाते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई।
- जमीन की उर्वरता में कमी: नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी, जिसके कारण दूसरी फसलें उगाना मुश्किल हो गया।
6. रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे?
उत्तर: रैयत नील की खेती से कतराते थे क्योंकि:
- कर्ज का जाल: बागान मालिक रैयतों को कर्ज देकर अनुबंध (सट्टा) के तहत नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। यह कर्ज चुकाने के लिए रैयत को बार-बार नील उगाना पड़ता था।
- कम आय: नील की फसल की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे रैयतों को नुकसान होता था।
- जमीन की हानि: नील की खेती से जमीन की उर्वरता खत्म हो जाती थी, जिसके कारण दूसरी फसलें नहीं उग पाती थीं।
- जबरदस्ती: बागान मालिक और गाँव के मुखिया रैयतों पर दबाव डालते थे कि वे नील की खेती करें, चाहे वे न चाहें।
7. किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया?
उत्तर: बंगाल में नील का उत्पादन इन कारणों से खत्म हो गया:
- जमीन की उर्वरता में कमी: नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी, जिससे दूसरी फसलें उगाना मुश्किल हो गया।
- कृत्रिम रंगों की खोज: 19वीं सदी में कृत्रिम रंगों की खोज के बाद नील की माँग कम हो गई।
- नील आयोग की सलाह: नील आयोग ने बागान मालिकों को जबरदस्ती करने का दोषी पाया और किसानों को सलाह दी कि वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं।
- किसानों का विरोध: किसानों ने बागान मालिकों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे चंपारण आंदोलन में।
आइए करके देखें
8. चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें।
उत्तर: चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ। यह भारत में ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ पहला बड़ा किसान आंदोलन था। उस समय नील बागान मालिक किसानों को कम कीमत पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। इससे किसानों की हालत बहुत खराब थी।
महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:
- किसानों को संगठित किया: गांधीजी चंपारण पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने गाँव-गाँव जाकर उनकी शिकायतें दर्ज कीं।
- सत्याग्रह और अहिंसा: गांधीजी ने सत्याग्रह और अहिंसा के तरीके से बागान मालिकों और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। यह भारत में उनका पहला सत्याग्रह था।
- किसानों का हौसला बढ़ाया: उन्होंने किसानों को एकजुट होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।
- नील आयोग का गठन: गांधीजी के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बनाया, जिसने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया। बागान मालिकों को जबरदस्ती बंद करने और किसानों को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
इस आंदोलन की सफलता के बाद गांधीजी को ‘महात्मा’ की उपाधि दी गई। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में एक बड़ा कदम था।
9. भारत के शुरुआती चाय या कॉफी बाग़ानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बाग़ानों में काम करने वाले मज़दूरों और नील के बाग़ानों में काम करने वाले मज़दूरों के जीवन में क्या समानताएँ या फ़र्क थे।
उत्तर:
भारत में चाय और कॉफी बागानों का इतिहास:
19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में चाय और कॉफी के बागान शुरू किए, खासकर असम, दार्जिलिंग और दक्षिण भारत में। चाय की खेती असम में 1830 के दशक में शुरू हुई, जबकि कॉफी बागान कर्नाटक और केरल में पहले से थे। इन बागानों के लिए मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाया गया। उन्हें बेहतर जीवन का वादा किया गया, लेकिन हकीकत में उनकी स्थिति बहुत खराब थी।
चाय/कॉफी और नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समानताएँ:
- शोषण: दोनों ही बागानों में मजदूरों का शोषण होता था। उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी और काम के घंटे बहुत लंबे थे।
- खराब रहन-सहन: मजदूरों को अस्वास्थ्यकर और तंग जगहों पर रहना पड़ता था।
- जबरदस्ती: नील की खेती के लिए किसानों को अनुबंध के जरिए मजबूर किया जाता था, जबकि चाय/कॉफी बागानों में मजदूरों को ठेका प्रणाली के तहत फँसाया जाता था।
- कर्ज का बोझ: दोनों ही मामलों में मजदूर कर्ज लेकर बंधुआ मजदूरी में फंस जाते थे।
फर्क:
- काम की प्रकृति: नील बागानों में किसान अपनी या किराए की जमीन पर खेती करते थे, जबकि चाय/कॉफी बागानों में मजदूर बागान मालिकों की जमीन पर काम करते थे।
- मजदूरों का स्थान: नील बागानों में ज्यादातर स्थानीय किसान काम करते थे, लेकिन चाय/कॉफी बागानों में मजदूरों को बिहार, उड़ीसा जैसे दूर के राज्यों से लाया जाता था।
- जमीन पर प्रभाव: नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी, जबकि चाय/कॉफी की खेती से जमीन पर ऐसा असर नहीं पड़ता था।
- आंदोलन: नील बागानों के खिलाफ चंपारण जैसे बड़े आंदोलन हुए, लेकिन चाय/कॉफी बागानों में मजदूरों के आंदोलन कम देखे गए।
