On this page we have shared the written Solutions for Bihar Board Class 8 History Chapter 4 – “आदिवासी, दीकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना”. These solutions are prepared by the subject experts and follows the new syllabus of Bihar Board. All question-answers are in Hindi medium.
यह अध्याय हमें आदिवासी समुदायों की जिंदगी और उनके संघर्षों की कहानी बताता है। हम जानेंगे कि कैसे वे झूम खेती, शिकार और पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे, और अंग्रेजों के शासन ने उनके जीवन को बदल दिया। यह भी समझ आएगा कि वन कानूनों और बाहरी लोगों (दीकुओं) के शोषण के खिलाफ आदिवासियों ने बगावत की, जिसमें बिरसा मुंडा जैसे नायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अध्याय से आपको आदिवासियों की संस्कृति और उनके स्वर्ण युग की कल्पना को समझने में मदद मिलेगी।
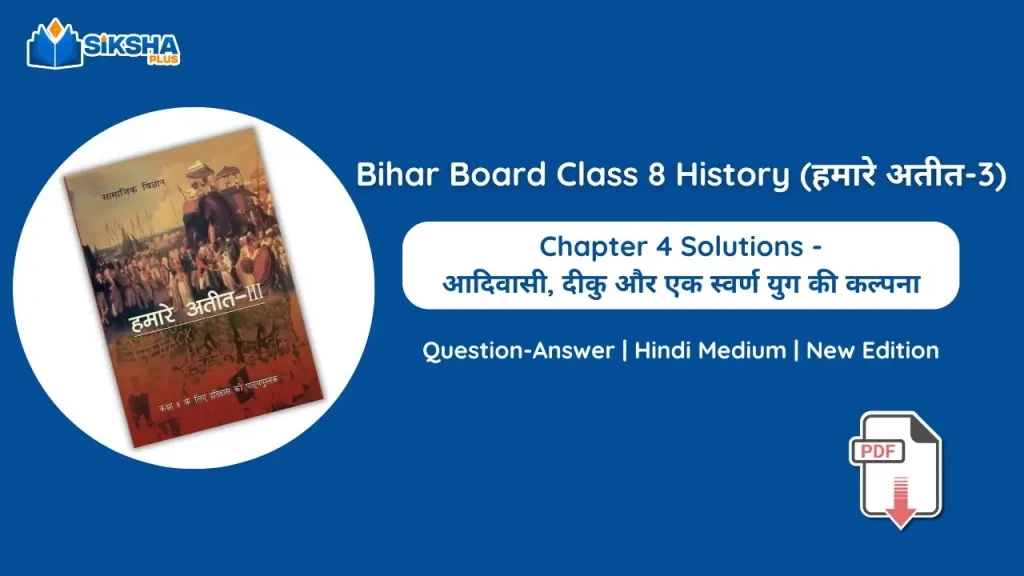
Bihar Board Class 8 History Chapter 4 Solutions
Contents
| Subject | History (हमारे अतीत-3) |
| Chapter | 4. आदिवासी, दीकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना |
| Class | 8th |
| Board | Bihar Board |
फिर से याद करें
1. रिक्त स्थान भरें –
(क) अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को …………… के रूप में वर्णित किया।
उत्तर: जंगली।
(ख) झूम खेती में बीज बोने के तरीके को …………… कहा जाता है।
उत्तर: छिटकना (पुक्कुटी)।
(ग) मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को …………… का स्वामित्व मिल गया।
उत्तर: जमींदारों।
(घ) असम के …………… और बिहार की …………… में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे।
उत्तर: चाय बागानों, कोयला खदानों।
2. सही या गलत बताएँ-
(क) झूम काश्तकार ज़मीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं।
उत्तर: गलत।
विश्लेषण: झूम खेती में काश्तकार ज़मीन की जुताई नहीं करते। वे जंगल की ज़मीन को साफ करते हैं, घास-फूस जलाते हैं, और बीज छिटकते हैं।
(ख) व्यापारी संथालों से कृमिकोष खरीदकर उसे पाँच गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे।
उत्तर: सही।
(ग) बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू-टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें।
उत्तर: सही।
(घ) अंग्रेज़ आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे।
उत्तर: गलत।
विश्लेषण: अंग्रेज़ों ने आदिवासियों की जीवनशैली को बदलने की कोशिश की और उनकी ज़मीन, जंगल और आजादी पर कब्जा किया।
आइए विचार करें
3. ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन-सी समस्याएँ थीं?
उत्तर: ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा:
- जंगल पर पाबंदी: घुमंतू काश्तकार जंगलों में खेती करते थे। वे पेड़ काटकर, घास जलाकर ज़मीन तैयार करते थे और बीज छिटकते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जंगलों पर कब्जा कर लिया और उनकी कटाई पर रोक लगा दी। इससे उनकी खेती करना मुश्किल हो गया।
- ज़मीन का नुकसान: अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीनें छीनकर व्यापारियों और जमींदारों को दे दीं। इससे काश्तकारों के पास खेती के लिए ज़मीन कम हो गई।
- नए नियम: अंग्रेज़ों ने घुमंतू खेती को गैरकानूनी घोषित कर दिया और काश्तकारों को एक जगह बसने के लिए मजबूर किया। इससे उनकी आजादी छिन गई।
- गरीबी और कर्ज: बिना ज़मीन और जंगल के, काश्तकारों को व्यापारियों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। इससे वे गरीबी और कर्ज में डूब गए।
4. औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए?
उत्तर: ब्रिटिश शासन से पहले आदिवासी मुखियाओं की बहुत ताकत थी। वे अपने समुदाय के नेता थे, ज़मीन और जंगल का प्रबंधन करते थे, और अपने नियम बनाते थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन में उनकी ताकत कम हो गई:
- शक्तियाँ छिन गईं: अंग्रेज़ों ने मुखियाओं की शासकीय ताकत छीन ली। वे अब अपने समुदाय के लिए नियम नहीं बना सकते थे।
- जमींदारी मिली: अंग्रेज़ों ने कुछ मुखियाओं को कई गाँवों की ज़मीन का मालिक बना दिया, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ों के नियम मानने पड़ते थे।
- नज़राना देना: मुखियाओं को अंग्रेज़ों को टैक्स या नज़राना देना पड़ता था।
- अनुशासन की ज़िम्मेदारी: अंग्रेज़ों ने मुखियाओं को अपने समुदाय को नियंत्रित करने का आदेश दिया, लेकिन उनकी पुरानी ताकत और सम्मान खत्म हो गया।
5. दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे?
उत्तर: आदिवासियों को दीकुओं (बाहरी लोगों) से गुस्सा होने के कई कारण थे:
- ज़मीन छीनी: दीकुओं ने आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, जिससे उनकी खेती और आजीविका प्रभावित हुई।
- आजादी का नुकसान: दीकुओं ने आदिवासियों की स्वतंत्रता छीन ली और उन्हें अपने नियमों के तहत जीने के लिए मजबूर किया।
- शोषण: व्यापारी और साहूकार दीकुओं ने आदिवासियों से सस्ते में सामान (जैसे कृमिकोष) खरीदा और उसे महंगे दाम पर बेचा।
- कर्ज और गरीबी: दीकुओं ने आदिवासियों को कर्ज दिया और ऊँची ब्याज दरें वसूलीं, जिससे वे गरीब हो गए।
- जंगल पर कब्जा: दीकुओं ने जंगलों पर कब्जा किया, जो आदिवासियों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा थे।
6. बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी?
उत्तर:
बिरसा का स्वर्ण युग: बिरसा ने एक ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना की, जहाँ मुंडा आदिवासी दीकुओं के शोषण से पूरी तरह आजाद हों। वे एक ऐसे सतयुग की बात करते थे, जब मुंडा लोग खुशहाल थे। उस समय वे खेती करते थे, तटबंध बनाते थे, झरनों को नियंत्रित करते थे, और पेड़-पौधे लगाते थे। वे आपस में झगड़ा नहीं करते थे और ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि उनके लोग शराब और अंधविश्वास छोड़कर फिर से वैसा जीवन जिएँ।
यह कल्पना आकर्षक क्यों थी?
बिरसा की स्वर्ण युग की बात लोगों को इसलिए पसंद आई क्योंकि:
- आजादी की उम्मीद: दीकुओं और अंग्रेज़ों के शोषण से तंग आदिवासियों को बिरसा की बातों से अपनी पुरानी आजादी और सम्मान वापस पाने की उम्मीद जगी।
- गर्व का अहसास: बिरसा ने उनके गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाई, जिससे लोगों को अपनी संस्कृति और इतिहास पर गर्व हुआ।
- बेहतर जीवन का सपना: बिरसा ने एक ऐसे जीवन का वादा किया, जहाँ कोई शोषण नहीं होगा और लोग शांति से रह सकेंगे।
- आध्यात्मिक प्रेरणा: बिरसा ने लोगों को शुद्ध जीवन जीने और गलत प्रथाओं को छोड़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे लोग उनके साथ जुड़ गए।
आइए करके देखें
7. अपने माता-पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके बीसवीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें। उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें।
उत्तर:
एक मशहूर आदिवासी विद्रोही थे ताना भगत, जो झारखंड के ओरांव समुदाय से थे। 1914 में, ताना भगत ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को शराब, मांस, और अंधविश्वास छोड़ने के लिए कहा। ताना भगत का मानना था कि सच्चाई और सादगी से जीने से आदिवासियों को आजादी मिलेगी। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया और कर (टैक्स) न देने की बात कही। उनकी यह लड़ाई आदिवासियों को एकजुट करने और उनके हक के लिए आवाज उठाने में बहुत महत्वपूर्ण थी।
8. भारत में रहने वाले किसी भी आदिवासी समूह को चुनें। उनके रीति-रिवाज़ और जीवन पद्धति का पता लगाएँ और देखें कि पिछले 50 साल के दौरान उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं?
उत्तर:
चुना गया समुदाय: गोंड आदिवासी (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं)।
रीति-रिवाज़ और जीवन पद्धति:
गोंड आदिवासियों की संस्कृति बहुत समृद्ध है। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे पेड़, पहाड़, और नदियाँ। उनके प्रमुख त्योहार हैं कर्मा और मड़ई, जहाँ वे नाचते-गाते हैं और अपने देवताओं को पूजते हैं। गोंड लोग पारंपरिक रूप से खेती, शिकार, और जंगल से लकड़ी व अन्य चीजें इकट्ठा करके जीवन चलाते थे। उनके घर मिट्टी और लकड़ी से बने होते हैं, और वे रंग-बिरंगे चित्र (गोंड कला) बनाते हैं, जो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। शादी और अन्य समारोहों में ढोल-नगाड़ों के साथ नाच-गाना होता है।
पिछले 50 साल में बदलाव:
- आधुनिक शिक्षा: पहले गोंड बच्चे स्कूल कम जाते थे, लेकिन अब स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने वाले गोंड युवा बढ़ रहे हैं।
- आजीविका: पहले गोंड लोग जंगल और खेती पर निर्भर थे, लेकिन अब कई लोग शहरों में मजदूरी या नौकरी करने लगे हैं।
- संस्कृति का प्रभाव: गोंड कला अब विश्व प्रसिद्ध है, और कई गोंड कलाकार अपनी कला को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ युवा आधुनिक जीवनशैली की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे पुराने रीति-रिवाज़ कम हो रहे हैं।
- ज़मीन का नुकसान: जंगल कटने और खनन जैसी गतिविधियों के कारण गोंड आदिवासियों की ज़मीन कम हुई है, जिससे उनकी पारंपरिक जीवनशैली प्रभावित हुई।
- आधुनिक सुविधाएँ: बिजली, सड़क, और मोबाइल फोन जैसी सुविधाएँ गोंड गाँवों में पहुँच रही हैं, जिससे उनका जीवन आसान हुआ, लेकिन उनकी पारंपरिक संस्कृति पर भी असर पड़ा।
गोंड आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकता और बाहरी दबावों ने उनके जीवन में बहुत बदलाव लाए हैं।
